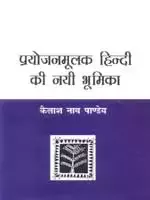|
भाषा एवं साहित्य >> प्रयोजनमूलक हिन्दी की नयी भूमिका प्रयोजनमूलक हिन्दी की नयी भूमिकाकैलाश नाथ पाण्डेय
|
325 पाठक हैं |
||||||
प्रयोजनमूलक हिन्दी की नयी भूमिका
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भाषा किसी भी देश की संस्कृति का अक्षय कोश होती है। यही परम्परा से
संस्कृति के विचारों को दोकर आधुनिकता से मिलाती है। वस्तुतः भाषा
जुम्मां-जुम्मां कह चुकने का अमूर्त्त माध्यम ही नहीं होती है, बल्कि खुद
को अपने समाज और परम्परा से जोड़े रखने का प्रेम-बंधन भी है। वह भटकाव और
गुमनामी के अंधेरे में आस्था की अक्षत् मशाल बन
‘गाइड’ की तरह
आगे-आगे चल राह दिखाती है। सौभाग्य से, भारतीय सर्जनात्मकता का अपराजेय
संकल्प हिन्दी उक्त सभी गुणों को जीती है। व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों
में बरती जाने वाली इस हिन्दी भाषा को भाषा-विज्ञानियों ने स्थूल रूप से
सामान्य और प्रयोजनमूलक इन दो भागों में विभक्त किया है। सुखद सूचना यह है
कि हिन्दी की इस नितांत ताजा-टटकी और कई संदर्भों में बेहद नयी
भाषिक-संरचना या नवजात शिशु रूप को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने
अपने-अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कर इसे सम्मानित किया है।
यह प्रयोजनमूलक हिन्दी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने एक ओर कम्प्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रमों, रक्षा, सेना, इन्जीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थानों, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, ए० एम० आई० के साथ विभिन्न संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों, चिट्ठी-पत्री, लेटर पैड़, स्टॉक-रजिस्टर, लिफाफे, मुहरें, नामपट्ट, स्टेशनरी के साथ-साथ कार्यालय-ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेस–विज्ञाप्ति, निविदा, नीलाम, अपील, केबलग्राम, मंजूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर यह कि पर्यटन बाजार, तीर्थस्थल, कल-कारखने, कचहरी आदि अब प्रयोजनमूलक हिन्दी की जद में आ गए हैं। हिन्दी के लिए यह शुभ है। अनेक विद्वानों के सहयोग से लिखी यह गंभीर कृति अपने पाठकों को संतुष्ट अवश्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
यह प्रयोजनमूलक हिन्दी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने एक ओर कम्प्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रमों, रक्षा, सेना, इन्जीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थानों, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, ए० एम० आई० के साथ विभिन्न संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों, चिट्ठी-पत्री, लेटर पैड़, स्टॉक-रजिस्टर, लिफाफे, मुहरें, नामपट्ट, स्टेशनरी के साथ-साथ कार्यालय-ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेस–विज्ञाप्ति, निविदा, नीलाम, अपील, केबलग्राम, मंजूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर यह कि पर्यटन बाजार, तीर्थस्थल, कल-कारखने, कचहरी आदि अब प्रयोजनमूलक हिन्दी की जद में आ गए हैं। हिन्दी के लिए यह शुभ है। अनेक विद्वानों के सहयोग से लिखी यह गंभीर कृति अपने पाठकों को संतुष्ट अवश्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
भूमिका
प्रबुद्धजन जानते हैं, भाषा गए वक्त की आवाज होती है। परम्परा और आधुनिकता के बीच वह पुल का काम करती है। वह संगति-विसंगति के साथ व्यक्ति के जीवन में घटित-उद्घाटित होने वाले प्रति संसार का बिम्ब होती है। वह राह होती है तो गति भी होती है। हिन्दी ने भाषा के उक्त तमाम गुणों को बखूबी जिया है। विरोधों के घटाटोप अधंकार में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इसने काफी कशमकश, लश्करकशी और जद्दोजहद किया। वस्तुतः ऊहा और आत्मग्रस्तता से बड़ी हद तक मुक्त हिन्दी न कभी थकी है, न निराश हुई है, इसे न समकालीन बेहद डरावनी और नंगी चुनौतियाँ खंडित और क्षरित कर पाई और न विरोध का ‘‘विक्षिप्त तथा रक्त से सना एवं हिंसा से भरा हुआ अतीत’’ ही डगमगा और विचलित कर पाया। परिणामतः विरोध की जड़ धूर्त्तता से तीखी मुठभेड़ लेती और पोर-पोर बनबना देने वाले देश को झेलती हिन्दी इस समय हर प्रदेश की मुक्त रूप में पुरलुफ्त सैर कर रही है। साफ शब्दों में, हिन्दी बोलने वाले इस समय देश में हर जगह फैले हुए हैं। आज यह विशाल भौगोलिक क्षेत्र की दुलरुई और प्रिय भाषा बन चुकी है। यह उपलब्धि इसे, इसके औघड़ अन्दाज और विलक्षण रचनात्मक संलग्नता की अकूत ताकत के कारण मिली हुई है।
डॉ० कैलाश नाथ पाण्डेय एक अर्से से मेरे आत्मीय लोगों में हैं। इनकी-कई-एक कृतियों को पढ़ा हूँ और इनके मौन श्रम से अभिभूत रहता हूँ। डॉ० पाण्डेय सही माने में मनस्वी हैं, मूक साधक हैं। धुर देहात में अवस्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय मलिकपुरा (गाजीपुर) में हिन्दी के प्राध्यापक हैं और शहर के एक छोर पर चुपचाप बस गए हैं। इनके दैनंदिन जीवन के साथ कोई कोलाहल नहीं जुड़ा है, जो बहुधा हर मनस्वी कृतिकार के साथ होता है। कम लोग होंगे, जिन्हें अपनी पुस्तकों का इतना भरोसा हो।
डॉ० पाण्डेय हिन्दी साहित्य के केवल अध्यापक ही नहीं हैं, आप भाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी के वर्तमान एवं भविष्य को लेकर गहरी चिन्ता और अध्ययन चिन्तन करने वाले विरल निष्ठावान लोगों में हैं। वर्तमान पुस्तक के अलावा इनकी अन्य दो कृतियाँ-‘‘उर्दूः दूसरी राजभाषा’’ (अनिल प्रकाशन, अलोपीबाग, इलाहाबाद 2003) और ‘‘हिन्दीः कुछ नयी चुनौतियाँ’’ (लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-2004) इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। बहुत दूर तक इनकी इस चिन्ता का मैं भी सहभोक्ता हूँ, लेकिन इस संदर्भ में मेरी कतिपय मुखर-असहमतियाँ भी हैं, शायद इस कारण कि मेरा आरम्भिक निर्माण हिन्दीतर मनीषा के परिवेश में हुआ है। केवल हिन्दी क्षेत्र में बसने-पलने वाले लोग इस प्रश्न की जटिलता से सामान्यता अपरिचित लगते हैं। फिर भी, मैं यह महसूस करता हूँ कि अगर राजभाषा और सामान्य जीवन में प्रयोजनमूलक या व्यावहारिक भाषा के रूप में हिन्दी को प्रभावी ढंग से प्रतिष्ठित होना है तो डॉ० पाण्डेय जैसे लोगों की सक्रिय निष्ठा के बलबूते ही संभव है।
वर्तमान पुस्तक ‘‘प्रयोजनमूलक हिन्दी की नयी भूमिका’’ को, दरअसल, पूर्व की उल्लिखित दोनों पुस्तकों के क्रम से ही पढ़ा-समझा जाना उचित होगा। पूर्व की दोनों ही पुस्तकें हिन्दी-उर्दू विवाद और राजभाषा के रूप में हिन्दी से जुड़े विभिन्न पक्षों को लेकर लिखी गई थीं और विपुल मूल दस्तावेजी सामग्री का उपयोग किया गया था। मतभेद के बावजूद पुस्तकों, के स्त्रोतों की प्रामाणिकता असंदिग्ध थी। कमी इतनी भर थी कि स्वर थोड़ा पालेमिकल’ और ‘रेटॉरिकल’ था, जिसके फलस्वरूप रेखापार की चिन्ताओं की अपेक्षित सहानुभूति को समझने की चेष्टा नहीं थी। वर्तमान पुस्तक के ‘‘आमुख’’ में भी लेखक ‘‘विरोध की जड़ धूर्त्तता’’ का उल्लेख करने से अपने को नहीं रोक सका है। इसका कारण अपने पक्ष के प्रति अतिशय लगाव या आत्यंतिक आश्वस्ति है। इसके बावजूद कुल मिलाकर, इस पुस्तक में लेखक हिन्दी के भविष्य के प्रति आश्वस्त है, जिसका प्रमाण न केवल इस पुस्तक में लेकर हिन्दी के भविष्य के प्रति आश्वस्वत है, जिसका प्रमाण न केवल राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृति बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हिन्दी का असरदार प्रवेश है। बकौल डॉ० पाण्डेय, ‘‘बाजार की भाषा बनकर बाजार का नक्शा और चरित्र को बगल ही दिया है, राष्ट्र की सरहदों को भी लाँघ लिया है। हिन्दी के लिए चीन अब हिमालय पार नहीं रहा, पाकिस्तानी बाजार में भी इसने अपने होने का परचम लहरा दिया है। समुद्र पार जाकर अब यह श्रीलंका और यूरोप के देशों में भी इन्टरनेट, ई-मेल और कम्प्यूटर के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। आज के बाजार के ‘ग्लोब’ में हिन्दी पूरी तरह ‘फिट’ हो चुकी हैं।’’
डॉ० पाण्डेय का यह विश्वास निराधार नहीं है। देखते-देखते अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकाएँ और दूरदर्शन के ‘चैनल्स’ हिन्दी को अपनाने के लिए विवश हुए हैं। व्यवसाय की दुनिया में 40-50 करोड़ वाले हिन्दी क्षेत्र को देर तक उपेक्षित या दरकिनार नहीं रखा जा सकता था।
1883 में हिन्दी नवजागरण के एक महापुरुष और हिन्दी भाषा के प्रबल पक्षकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के लिए भी खड़ी बोली हिन्दी अभी पश्चिम से आयी एक ‘‘परदेशी भाषा’’ थी, जिसे उन्होंने काव्य रचना के योग्य नहीं माना था, लेकिन हिन्दू-मुस्लिम मेल की व्यावहारिक विवशताओं से जन्मी खड़ी बोली हिन्दी का दिल्ली आगरा, मथुरा इत्यादि की मंडियों के माध्यम से अपना विस्तार हुआ और वह एक विराट क्षेत्र की भाषा बन गई। ब्रज, अवधी, मैथिल जैसी अनेकानेक प्राचीन और साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध जनभाषाओं की सीमाओं को अतिक्रांत करती अंततः यह लगभग समूचे उत्तर भारत की लिंगुआफ्रांका’ बन गई। डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषा शास्त्री को इस भाषायी परिघटना का कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं सूझता और डॉ० रामविलास शर्मा इसे हिन्दी की अपनी परिघटना का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं सूझता और डॉ. रामविलास शर्मा इसे हिन्दी की अपनी आंतरिक उर्जा की अभिव्यक्ति मानकर अभिभूत हैं। हिन्दी का विकास और विस्तार राजभाषा के रूप में नहीं, बल्कि व्यावहारिक जनभाषा के रूप में ही हुआ है। मूलतः यह सत्ता की भाषा नहीं, बल्कि प्रतिवाद की भाषा है। यह सत्तापरक विवशता की देन नहीं, बल्कि व्यवहारपरक विवशता की उपज है। यही इसकी अपराजेयता की कुंजी है। डॉ. पाण्डेय का ध्यान भी हिन्दी की प्रयोजनमूलकता पर केन्द्रित हैं, क्योंकि प्रयोजन के नए-नए क्षेत्रों तक इसकी पहुँच आवश्यक है। सिद्धातः राजभाषा के रूप में और व्यवहारतः बाजार-व्यवहार की भाषा के रूप में इसे स्पष्ट स्वीकृति मिल चुकी हैं। अब प्रश्न ज्ञान और व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग हेतु मानकीकृत शब्दावली का है। डॉ० पाण्डेय की यह पुस्तक इस दिशा में एक गंभीर प्रयास है।
पुस्तक के शीर्षक का ‘नयी’ विशेषण विशेष रूप से ध्यान खींचता है। एक दौर था, जब हिन्दी उत्तर भारत की प्रमुख मंडियों की भाषा थी। धीरे-धीरे यह साहित्य की भाषा बनी, लेकिन इस मंडी की भाषा साहित्य की भाषा के बीच का सेतु बहुत कमजोर था। मंडी की भाषा के रूप में इसमें जमीनी अनगढ़ता थी और पारम्परिक संस्कृतनिष्ठ साहित्यकारों के चलते साहित्य की भाषा के रूप में यह तत्समता से बोझिल और अबूझ थी। कोई इसका संस्कृतकरण करता था, तो कोई फारसीकरण। ये दोनों ही रूप आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और बाजार की विविध विशेषीकृत आवश्यकताओं की दृष्टि से अपर्याप्त थे, लेकिन राजभाषा के रूप में स्वीकृति के पश्चात इसका दायित्व व्यापक बना। अब यह आधुनिक प्रशासन, ज्ञान-विज्ञान, तकनीक और बाजार के संभार से बच नहीं सकती थी। अब इसे टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर, टेलेक्स, शेयर बाजार इत्यादि की भाषा से भी रूबरू होना था। डॉ० पाण्डेय इसकी अद्यतन उपलब्धियों के प्रति भी जागरूक हैं,-‘‘इसने बाजार तथा आधुनिकता के दबाव के कारण गाँव के हाट-बाजार, गली-चौराहे, कल-कारखाने, कचहरी तथा सब्जी मंडियों में भी अपने आगमन की सूचना साइनबोर्डों पर छपे विज्ञापनों तथा अन्यान्य तरीकों से दी है’’, अर्थात् ज्ञान एवं व्यवहार के नए-नए खुलते क्षितिजों से जन्मी अपेक्षाओं के संदर्भ में भी हिन्दी ने अपनी अर्थवत्ता का एहसास कराया है। कम-से-कम पाण्डेय जी तो आश्वस्त हैं ही।
डॉ० कैलाश नाथ पाण्डेय एक अर्से से मेरे आत्मीय लोगों में हैं। इनकी-कई-एक कृतियों को पढ़ा हूँ और इनके मौन श्रम से अभिभूत रहता हूँ। डॉ० पाण्डेय सही माने में मनस्वी हैं, मूक साधक हैं। धुर देहात में अवस्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय मलिकपुरा (गाजीपुर) में हिन्दी के प्राध्यापक हैं और शहर के एक छोर पर चुपचाप बस गए हैं। इनके दैनंदिन जीवन के साथ कोई कोलाहल नहीं जुड़ा है, जो बहुधा हर मनस्वी कृतिकार के साथ होता है। कम लोग होंगे, जिन्हें अपनी पुस्तकों का इतना भरोसा हो।
डॉ० पाण्डेय हिन्दी साहित्य के केवल अध्यापक ही नहीं हैं, आप भाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी के वर्तमान एवं भविष्य को लेकर गहरी चिन्ता और अध्ययन चिन्तन करने वाले विरल निष्ठावान लोगों में हैं। वर्तमान पुस्तक के अलावा इनकी अन्य दो कृतियाँ-‘‘उर्दूः दूसरी राजभाषा’’ (अनिल प्रकाशन, अलोपीबाग, इलाहाबाद 2003) और ‘‘हिन्दीः कुछ नयी चुनौतियाँ’’ (लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-2004) इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। बहुत दूर तक इनकी इस चिन्ता का मैं भी सहभोक्ता हूँ, लेकिन इस संदर्भ में मेरी कतिपय मुखर-असहमतियाँ भी हैं, शायद इस कारण कि मेरा आरम्भिक निर्माण हिन्दीतर मनीषा के परिवेश में हुआ है। केवल हिन्दी क्षेत्र में बसने-पलने वाले लोग इस प्रश्न की जटिलता से सामान्यता अपरिचित लगते हैं। फिर भी, मैं यह महसूस करता हूँ कि अगर राजभाषा और सामान्य जीवन में प्रयोजनमूलक या व्यावहारिक भाषा के रूप में हिन्दी को प्रभावी ढंग से प्रतिष्ठित होना है तो डॉ० पाण्डेय जैसे लोगों की सक्रिय निष्ठा के बलबूते ही संभव है।
वर्तमान पुस्तक ‘‘प्रयोजनमूलक हिन्दी की नयी भूमिका’’ को, दरअसल, पूर्व की उल्लिखित दोनों पुस्तकों के क्रम से ही पढ़ा-समझा जाना उचित होगा। पूर्व की दोनों ही पुस्तकें हिन्दी-उर्दू विवाद और राजभाषा के रूप में हिन्दी से जुड़े विभिन्न पक्षों को लेकर लिखी गई थीं और विपुल मूल दस्तावेजी सामग्री का उपयोग किया गया था। मतभेद के बावजूद पुस्तकों, के स्त्रोतों की प्रामाणिकता असंदिग्ध थी। कमी इतनी भर थी कि स्वर थोड़ा पालेमिकल’ और ‘रेटॉरिकल’ था, जिसके फलस्वरूप रेखापार की चिन्ताओं की अपेक्षित सहानुभूति को समझने की चेष्टा नहीं थी। वर्तमान पुस्तक के ‘‘आमुख’’ में भी लेखक ‘‘विरोध की जड़ धूर्त्तता’’ का उल्लेख करने से अपने को नहीं रोक सका है। इसका कारण अपने पक्ष के प्रति अतिशय लगाव या आत्यंतिक आश्वस्ति है। इसके बावजूद कुल मिलाकर, इस पुस्तक में लेखक हिन्दी के भविष्य के प्रति आश्वस्त है, जिसका प्रमाण न केवल इस पुस्तक में लेकर हिन्दी के भविष्य के प्रति आश्वस्वत है, जिसका प्रमाण न केवल राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृति बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हिन्दी का असरदार प्रवेश है। बकौल डॉ० पाण्डेय, ‘‘बाजार की भाषा बनकर बाजार का नक्शा और चरित्र को बगल ही दिया है, राष्ट्र की सरहदों को भी लाँघ लिया है। हिन्दी के लिए चीन अब हिमालय पार नहीं रहा, पाकिस्तानी बाजार में भी इसने अपने होने का परचम लहरा दिया है। समुद्र पार जाकर अब यह श्रीलंका और यूरोप के देशों में भी इन्टरनेट, ई-मेल और कम्प्यूटर के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। आज के बाजार के ‘ग्लोब’ में हिन्दी पूरी तरह ‘फिट’ हो चुकी हैं।’’
डॉ० पाण्डेय का यह विश्वास निराधार नहीं है। देखते-देखते अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकाएँ और दूरदर्शन के ‘चैनल्स’ हिन्दी को अपनाने के लिए विवश हुए हैं। व्यवसाय की दुनिया में 40-50 करोड़ वाले हिन्दी क्षेत्र को देर तक उपेक्षित या दरकिनार नहीं रखा जा सकता था।
1883 में हिन्दी नवजागरण के एक महापुरुष और हिन्दी भाषा के प्रबल पक्षकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के लिए भी खड़ी बोली हिन्दी अभी पश्चिम से आयी एक ‘‘परदेशी भाषा’’ थी, जिसे उन्होंने काव्य रचना के योग्य नहीं माना था, लेकिन हिन्दू-मुस्लिम मेल की व्यावहारिक विवशताओं से जन्मी खड़ी बोली हिन्दी का दिल्ली आगरा, मथुरा इत्यादि की मंडियों के माध्यम से अपना विस्तार हुआ और वह एक विराट क्षेत्र की भाषा बन गई। ब्रज, अवधी, मैथिल जैसी अनेकानेक प्राचीन और साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध जनभाषाओं की सीमाओं को अतिक्रांत करती अंततः यह लगभग समूचे उत्तर भारत की लिंगुआफ्रांका’ बन गई। डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषा शास्त्री को इस भाषायी परिघटना का कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं सूझता और डॉ० रामविलास शर्मा इसे हिन्दी की अपनी परिघटना का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं सूझता और डॉ. रामविलास शर्मा इसे हिन्दी की अपनी आंतरिक उर्जा की अभिव्यक्ति मानकर अभिभूत हैं। हिन्दी का विकास और विस्तार राजभाषा के रूप में नहीं, बल्कि व्यावहारिक जनभाषा के रूप में ही हुआ है। मूलतः यह सत्ता की भाषा नहीं, बल्कि प्रतिवाद की भाषा है। यह सत्तापरक विवशता की देन नहीं, बल्कि व्यवहारपरक विवशता की उपज है। यही इसकी अपराजेयता की कुंजी है। डॉ. पाण्डेय का ध्यान भी हिन्दी की प्रयोजनमूलकता पर केन्द्रित हैं, क्योंकि प्रयोजन के नए-नए क्षेत्रों तक इसकी पहुँच आवश्यक है। सिद्धातः राजभाषा के रूप में और व्यवहारतः बाजार-व्यवहार की भाषा के रूप में इसे स्पष्ट स्वीकृति मिल चुकी हैं। अब प्रश्न ज्ञान और व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग हेतु मानकीकृत शब्दावली का है। डॉ० पाण्डेय की यह पुस्तक इस दिशा में एक गंभीर प्रयास है।
पुस्तक के शीर्षक का ‘नयी’ विशेषण विशेष रूप से ध्यान खींचता है। एक दौर था, जब हिन्दी उत्तर भारत की प्रमुख मंडियों की भाषा थी। धीरे-धीरे यह साहित्य की भाषा बनी, लेकिन इस मंडी की भाषा साहित्य की भाषा के बीच का सेतु बहुत कमजोर था। मंडी की भाषा के रूप में इसमें जमीनी अनगढ़ता थी और पारम्परिक संस्कृतनिष्ठ साहित्यकारों के चलते साहित्य की भाषा के रूप में यह तत्समता से बोझिल और अबूझ थी। कोई इसका संस्कृतकरण करता था, तो कोई फारसीकरण। ये दोनों ही रूप आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और बाजार की विविध विशेषीकृत आवश्यकताओं की दृष्टि से अपर्याप्त थे, लेकिन राजभाषा के रूप में स्वीकृति के पश्चात इसका दायित्व व्यापक बना। अब यह आधुनिक प्रशासन, ज्ञान-विज्ञान, तकनीक और बाजार के संभार से बच नहीं सकती थी। अब इसे टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर, टेलेक्स, शेयर बाजार इत्यादि की भाषा से भी रूबरू होना था। डॉ० पाण्डेय इसकी अद्यतन उपलब्धियों के प्रति भी जागरूक हैं,-‘‘इसने बाजार तथा आधुनिकता के दबाव के कारण गाँव के हाट-बाजार, गली-चौराहे, कल-कारखाने, कचहरी तथा सब्जी मंडियों में भी अपने आगमन की सूचना साइनबोर्डों पर छपे विज्ञापनों तथा अन्यान्य तरीकों से दी है’’, अर्थात् ज्ञान एवं व्यवहार के नए-नए खुलते क्षितिजों से जन्मी अपेक्षाओं के संदर्भ में भी हिन्दी ने अपनी अर्थवत्ता का एहसास कराया है। कम-से-कम पाण्डेय जी तो आश्वस्त हैं ही।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book